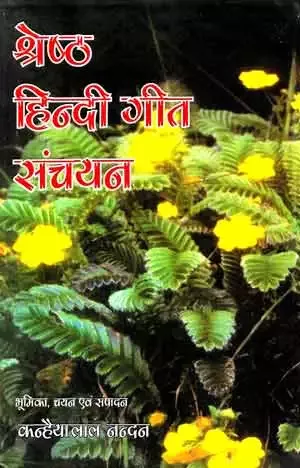|
कविता संग्रह >> श्रेष्ठ हिन्दी गीत संचयन श्रेष्ठ हिन्दी गीत संचयनकन्हैयालाल नंदन
|
339 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत संचयन विगत शताब्दी के गीतों का एक प्रतिनिधि समुच्चय है, जिसमें मैथिलीशरण गुप्त के गीतों से लेकर हिन्दी गीत के अद्यतन रूप तक की बानगी पाठकों को एक जगह मिल सकेगी।
Shreshth Hindi Geet Sanchyan - A hindi Book by - K. L. Nandan श्रेष्ठ हिन्दी गीत संचयन - कन्हैयालाल नंदन
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मुक्तक के एक प्रभेद के रूप में गीत शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र और अमरकोश में इसका उल्लेख है। आधुनिक युग में जिस भावबोध और शैली के गीत लिखे गये, वे सीधे भारतीय गीत परंपरा से यानी वैदिक सामगीतों, बौद्ध थेरीगाथाओं, सिद्धों के चर्यापदों और सन्तों-भक्तों की पदावलियों से अनुप्रेरित रहे हैं। आधुनिक गीतों का जन्म, भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण के युग में पश्चिमी अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से उद्भूत स्वच्छन्दतावाद-रोमांटिसिज्म-से हुआ है। इसके निर्माण में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विराट व्यक्तित्त्व, विश्वजनीन मानवतावादी दृष्टि और उसको अभिव्यक्त करने के लिए नवनिर्मित भाषा, शब्दावली गीत-प्रणाली और संगीत-पद्धति का अमूल्य योगदान रहा। सामान्यतः 1920 से 1936 तक के कालखण्ड को छायावादी युग कहा जाता है। इसे हिन्दी गीतों का स्वर्णयुग भी माना गया। गीत विधा इसी युग में प्रौढ़ता को प्राप्त हुई। प्रायः सभी कवियों ने गीत विधा को अपने अनुभूतियों की अभिव्यंजना का माध्यम बनाया। छायावादी कला आत्माभिव्यंजक रही और शिल्प गीतात्मक...क्या विचार..क्या दर्शन..क्या शैली और क्या भाषा..इन सभी में जैसे सम्पूर्ण युग अपने पूर्ववर्ती युग से विशिष्ट और अप्रतिम हो उठा।
प्रस्तुत संचयन विगत शताब्दी के गीतों का एक प्रतिनिधि समुच्चय है, जिसमें मैथिलीशरण गुप्त के गीतों से लेकर हिन्दी गीत के अद्यतन रूप तक की बानगी पाठकों को एक जगह मिल सकेगी। गीत की यह अनवरत यात्रा लम्बी भूमिका से समृद्ध है, जो हिन्दी गीत पर कार्यरत शिक्षार्थियों के शोध के लिए उतनी ही उपयोगी है, जितनी गीत प्रेमियों के पठन के लिए। हिन्दी कविता प्रचलित मुहावरों को गीत में किस तरह इस्तेमाल करती रही, छायावाद युग ने हिन्दी गीत को जो पुष्ट आधार दिया, उसमें परवर्ती गीत ने अपने समसामयिक जीवन को किस तरह रूपायित किया, इसे जानने के लिए यह संचयन एक अनिवार्य सन्दर्भ ग्रंन्थ है। संकलन में एक सौ नब्बे कवियों के सवा तीन सौ गीतों की श्रेष्ठता पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रतिष्ठित रही है। किन्तु जिन्हें एक जगह पा सकना असम्भव था।
प्रस्तुत संचयन विगत शताब्दी के गीतों का एक प्रतिनिधि समुच्चय है, जिसमें मैथिलीशरण गुप्त के गीतों से लेकर हिन्दी गीत के अद्यतन रूप तक की बानगी पाठकों को एक जगह मिल सकेगी। गीत की यह अनवरत यात्रा लम्बी भूमिका से समृद्ध है, जो हिन्दी गीत पर कार्यरत शिक्षार्थियों के शोध के लिए उतनी ही उपयोगी है, जितनी गीत प्रेमियों के पठन के लिए। हिन्दी कविता प्रचलित मुहावरों को गीत में किस तरह इस्तेमाल करती रही, छायावाद युग ने हिन्दी गीत को जो पुष्ट आधार दिया, उसमें परवर्ती गीत ने अपने समसामयिक जीवन को किस तरह रूपायित किया, इसे जानने के लिए यह संचयन एक अनिवार्य सन्दर्भ ग्रंन्थ है। संकलन में एक सौ नब्बे कवियों के सवा तीन सौ गीतों की श्रेष्ठता पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रतिष्ठित रही है। किन्तु जिन्हें एक जगह पा सकना असम्भव था।
गीत : एक अनवरत नदी
(गीत की अविराम यात्रा)
गीत की जब भी बात उठती है, तो मुझे उमाकांत मालवीय अपनी पंक्ति के साथ याद आते हैं कि ‘गीत एक अनवरत नदी है’। उन्होंने कहा कि इस अनवरत धार में नेकी और बदी दोनों बहते हैं। उन्होंने गीत में पत्थर के पिघलते मसौदे भी देखे, पत्थर पर उगे तुलसी के पौदे भी और अनवरत प्रवाहमान धारा की लहर में उन्हें किरणों के वलय कौंधते हुए दीखे। इतना ही नहीं, इसकी उदामत्ता को उन्होंने सूफ़ी संत सरमद की अनलहक़ की पुकार का पर्याय तक बताया।
गीत की लंबी यात्रा में तमाम रूप देखने को मिलते हैं। यह भी बताऊँ कि उमाकांत मालवीय अकेले रचनाकार नहीं हैं। उनके आगे भी और पीछे भी एक लंबी सरणि है, जिसने गति के अभ्यंतर को शब्दों में रूपायित करने की चेष्टा की है। इंदिरा गौड़ ने तो स्त्री-पुरुष के समूचे प्रकृत संबंधों को गीत के रूप में ही देखा है और कहा है :
गीत की लंबी यात्रा में तमाम रूप देखने को मिलते हैं। यह भी बताऊँ कि उमाकांत मालवीय अकेले रचनाकार नहीं हैं। उनके आगे भी और पीछे भी एक लंबी सरणि है, जिसने गति के अभ्यंतर को शब्दों में रूपायित करने की चेष्टा की है। इंदिरा गौड़ ने तो स्त्री-पुरुष के समूचे प्रकृत संबंधों को गीत के रूप में ही देखा है और कहा है :
‘‘गुनगुनाओ तो सही तुम तनिक मुझको
मैं तुम्हारे गीत का पहला चरण हूँ।’’
मैं तुम्हारे गीत का पहला चरण हूँ।’’
मेरे समकालीन रचनाकार सोम ठाकुर ने गीत को ‘समन्दर के ज़िन्दा रतन’ कहा है :
‘‘कल्पवृक्षों के सुनहरे फूल हैं ये
दर्द की आकाशवाणी के वचन हैं
तू इन्हें दिल के खज़ाने में सँजो ले
गीत ये ज़िन्दा समन्दर के रतन हैं।
रामगिरि के यक्ष से ये कब अलग हैं
और कब दमयंतियों से दूर हैं ये
ज़हर का प्याला पिये सुकरात हैं ये
ख़ुद ब ख़ुद सूली चढ़े मंसूर हैं ये
छोड़ने पर भी न छूटेंगे कभी, ये
भावना के मुँह लगे आदिम व्यसन हैं;
दर्द की आकाशवाणी के वचन हैं
तू इन्हें दिल के खज़ाने में सँजो ले
गीत ये ज़िन्दा समन्दर के रतन हैं।
रामगिरि के यक्ष से ये कब अलग हैं
और कब दमयंतियों से दूर हैं ये
ज़हर का प्याला पिये सुकरात हैं ये
ख़ुद ब ख़ुद सूली चढ़े मंसूर हैं ये
छोड़ने पर भी न छूटेंगे कभी, ये
भावना के मुँह लगे आदिम व्यसन हैं;
...ये समय के सत्य से उलझे सपन हैं।’’
सोम की इन पंक्तियों में गीत में अभिव्यक्त राग-विराग, दर्शन, चिंतन, सत्यान्वेषण, भावना के उद्देश्य के छलकते रसघट, आनन्द की अजस्त्र बहती धारा, प्रेमपर्वों पर आँसुओं के घाट पर गूँजते भजनों और सूनेपन की वीथियों में भटकी हुई बयार......इस सबका आभास एक साथ हो जाती है। निराला ने लिखा था :
सोम की इन पंक्तियों में गीत में अभिव्यक्त राग-विराग, दर्शन, चिंतन, सत्यान्वेषण, भावना के उद्देश्य के छलकते रसघट, आनन्द की अजस्त्र बहती धारा, प्रेमपर्वों पर आँसुओं के घाट पर गूँजते भजनों और सूनेपन की वीथियों में भटकी हुई बयार......इस सबका आभास एक साथ हो जाती है। निराला ने लिखा था :
‘‘गरज गरज घन अंधकारों में गा अपने संगीत
बंधु, वे बाधा बंधविहीन
आँखों में नवजीवन का तू अंजन लगा पुनीत
बिखर झर जाने दे प्राचीन
....भर उद्दाम वेग से बाधा हर तू कर्कश प्राणट
दूर कर दुर्बल नि:श्वास
किरणों की गति से आ आ तू, गा तू गौरवगान
एक कर दे पृथ्वी आकाश।’’
बंधु, वे बाधा बंधविहीन
आँखों में नवजीवन का तू अंजन लगा पुनीत
बिखर झर जाने दे प्राचीन
....भर उद्दाम वेग से बाधा हर तू कर्कश प्राणट
दूर कर दुर्बल नि:श्वास
किरणों की गति से आ आ तू, गा तू गौरवगान
एक कर दे पृथ्वी आकाश।’’
उन्होंने माना था कि गीत में वह शक्ति है, जो किरणों की गति से आकर पृथ्वी और आकाश को एक कर देने की क्षमता रखती है।
अपार क्षमतावाली इस काव्य विधा की छवियाँ विविधवर्णी हैं; गति कर्म का उद्बोधन है, प्रेम का आत्मनिवेदन है, संवेदना की मानक छवि है, रागात्मकता का प्रतिफलन है, विडंबनाओं की प्रतिध्वनि है। संभवत: कविता का आदिम रूप है, जिसे मनुष्य मात्र की मातृभाषा कहा जा सकता है। कोई ऐसा मानव समुदाय नहीं, जिसका अपना गीत, संगीत और नृत्य का विशिष्ट भंडार न हो। गीत, संगीत और कविता के बीच भिन्नता दर्शाने वाली काव्यशास्त्रीय परिभाषाएँ बहुत प्राचीन नहीं हैं, यों कविता मनुष्य का शब्द जीवन भी है। मानव सभ्यता के प्रारम्भिक सरलतम रूप-गुफ़ावास या घुमंतू जीवन से लेकर आज इक्कीसवीं सदी में प्रविष्ट हो चुके कम्प्यूटर संचालित वैश्वीकृत जटिलतम महानगरीय जीवन तक में आत्माभिव्यक्ति, आत्मप्रकाशन और संचरण मानव-जीवन और चिति का अभिन्न अंग है, उसकी अपरिहार्य आवश्यकता है।
मानव-विकास के आदि क्रम में अभियक्ति नादात्मक रही होगी और संगीत और गीत दोनों की उत्पत्ति नाद से हुई होगी। निश्चय ही आदिम व्यवस्था में शब्दों का भंडार और ज्ञान की मात्रा अल्प ही रहे होंगे। व्यक्तिगत और सामुदायिक अनुभव जगत और प्रतिक्रियाएँ भी लगभग अपृथक् रहे होंगे और उन्हीं से उठा हुआ लोकगीत क़रीब-क़रीब उतना ही सहज, उत्स्फूर्त और मार्मिक रहा होगा, जितना कि कोकिल का पंचम स्वर, बुलबुल का दर्दीला गान और मयूर का नृत्यमय केका-स्वर। गीत के साथ नाद और गेयता का संबंध उसकी संज्ञा और संरचना में ही अनुस्यूत है। ऐसा नहीं कि गाये बिना गीत नहीं रहता, लेकिन गेयता उसकी प्रकृति का अंग है और इसी प्रकृति को रेखांकित करते हुए जगदीश गुप्त ने लिखा है कि ‘‘लोकगीतों से लेकर सिने गीतों तक भारतीय जनमानस को गीत कहीं इतना गहराई से जकड़े हुए है कि उसका स्वर कैसा भी हो, वह उसे ग्राह्य हो जाता है।’’
इन स्वरों में व्यक्ति की साझेदारी सामाजिक संरचना को भी रेखांकित करती रही। समाज-रचना और मानव-जीवन में जटिलताओं के बनते जाने की वजह से लोकगीतों की प्राकृतिक सहजता तो धीरे-धीरे कुण्ठित होती रही, लेकिन साथ ही मनुष्य की भाषा-सम्पदा बढ़ने, अनुभूति-संसार में अभिवृद्धि होने और व्यापकता आने की वजह से लोकगीतों के समानान्तर ही कलागीतों की भी रचना होने लगी। लेकिन यह सुखद स्थिति रही कि अपने मूल स्रोत्र की सहजता, संगीतात्मकता और भावात्मकता की विरासत को उसने पूरी तरह गवाँ नहीं दिया, वरन् उसे एक नए रूप में, परिष्कृत कर प्रस्तुत कर दिया। नाद, लय, छन्द के रूप में संगीतात्मकता कविता की पूरी बुनावट में बनी रही, इसीलिए वह सदैव अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रख पायी। विश्व-विख्यात कवि-कथाकार एडगर एलन पो ने कहा है, ‘‘संगीत का जब किसी प्रीतिकार कल्पना से संयोग होता है, तो वह कविता बन जाती है। संगीतरहित कल्पना, अपनी स्पष्टता अथवा निश्चितता के कारण गद्य का रूप धारण कर लेती है।’’ चूँकि मन की गहनतम भावना का संगीत से निकट का संबंध है, इसीलिए संगीत समीक्षक मीयर ने यहाँ तक कहा कि ‘‘कविता संगीत है और संगीत ध्वनिमय कविता !’’ हालाँकि यह निष्कर्ष सामान्य कविता पर भी लागू होता है, लेकिन वस्तुत: गीत ही इस कसौटी पर सर्वाधिक खरा उतरता है।
मीयर की यह धारणा भी विचारणीय है कि ‘‘कविता, आदिम मानव की सहज, अविवक्षित चिल्लाहट या पुकार मात्र थी। भय, उल्लास, आश्चर्य, अवसाद या प्रेम के अप्रत्याशित आवेश को लयबद्ध ध्वनियों या गीत-क्रमों में अभिव्यक्त किया जाने लगा और यही कविता का आदि स्वरूप था। ये ध्वनियाँ मूल रूप में शब्दार्थविहीन थीं। बाद के युग में विकसित गीतों में उनके अवशेष, उन्हीं के बीच समाविष्ट हो गये।’’
कविता में गीत को ‘आवेगमय भावनाओं का स्वत:स्फूर्त उफान’ भी कहा गया है। अंग्रेज़ी के सुप्रसिद्ध कवि पी.बी. शेली ने कहा है, ‘‘काव्य कोई तर्क-शक्ति नहीं, जो स्वेच्छापूर्वक काम में लायी जा सके। कोई कवि यह नहीं कह सकता कि मैं कविता रचूँगा, बड़ा कवि तो और भी ऐसी बात नहीं कह सकता। रचना करने वाली शक्ति तो भीतर वे वैसे ही आती है, जैसे फूल का रंग फूल के विकास के साथ-साथ ढलता और बदलता रहता है तथा हमारी चेतन शक्तियाँ, उस अदृश्य प्रभाव का न आना जानती है और न जाना।’’ और इसीलिए कवि-कर्म आसान नहीं। सर्वसुलभ भी नहीं। यह क्षमता सहज उपलब्ध नहीं होती, उसके लिए गहन-सघन, अनवरत साधना की आवश्यकता होती है। तपना पड़ता है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन में कहा भी है :
अपार क्षमतावाली इस काव्य विधा की छवियाँ विविधवर्णी हैं; गति कर्म का उद्बोधन है, प्रेम का आत्मनिवेदन है, संवेदना की मानक छवि है, रागात्मकता का प्रतिफलन है, विडंबनाओं की प्रतिध्वनि है। संभवत: कविता का आदिम रूप है, जिसे मनुष्य मात्र की मातृभाषा कहा जा सकता है। कोई ऐसा मानव समुदाय नहीं, जिसका अपना गीत, संगीत और नृत्य का विशिष्ट भंडार न हो। गीत, संगीत और कविता के बीच भिन्नता दर्शाने वाली काव्यशास्त्रीय परिभाषाएँ बहुत प्राचीन नहीं हैं, यों कविता मनुष्य का शब्द जीवन भी है। मानव सभ्यता के प्रारम्भिक सरलतम रूप-गुफ़ावास या घुमंतू जीवन से लेकर आज इक्कीसवीं सदी में प्रविष्ट हो चुके कम्प्यूटर संचालित वैश्वीकृत जटिलतम महानगरीय जीवन तक में आत्माभिव्यक्ति, आत्मप्रकाशन और संचरण मानव-जीवन और चिति का अभिन्न अंग है, उसकी अपरिहार्य आवश्यकता है।
मानव-विकास के आदि क्रम में अभियक्ति नादात्मक रही होगी और संगीत और गीत दोनों की उत्पत्ति नाद से हुई होगी। निश्चय ही आदिम व्यवस्था में शब्दों का भंडार और ज्ञान की मात्रा अल्प ही रहे होंगे। व्यक्तिगत और सामुदायिक अनुभव जगत और प्रतिक्रियाएँ भी लगभग अपृथक् रहे होंगे और उन्हीं से उठा हुआ लोकगीत क़रीब-क़रीब उतना ही सहज, उत्स्फूर्त और मार्मिक रहा होगा, जितना कि कोकिल का पंचम स्वर, बुलबुल का दर्दीला गान और मयूर का नृत्यमय केका-स्वर। गीत के साथ नाद और गेयता का संबंध उसकी संज्ञा और संरचना में ही अनुस्यूत है। ऐसा नहीं कि गाये बिना गीत नहीं रहता, लेकिन गेयता उसकी प्रकृति का अंग है और इसी प्रकृति को रेखांकित करते हुए जगदीश गुप्त ने लिखा है कि ‘‘लोकगीतों से लेकर सिने गीतों तक भारतीय जनमानस को गीत कहीं इतना गहराई से जकड़े हुए है कि उसका स्वर कैसा भी हो, वह उसे ग्राह्य हो जाता है।’’
इन स्वरों में व्यक्ति की साझेदारी सामाजिक संरचना को भी रेखांकित करती रही। समाज-रचना और मानव-जीवन में जटिलताओं के बनते जाने की वजह से लोकगीतों की प्राकृतिक सहजता तो धीरे-धीरे कुण्ठित होती रही, लेकिन साथ ही मनुष्य की भाषा-सम्पदा बढ़ने, अनुभूति-संसार में अभिवृद्धि होने और व्यापकता आने की वजह से लोकगीतों के समानान्तर ही कलागीतों की भी रचना होने लगी। लेकिन यह सुखद स्थिति रही कि अपने मूल स्रोत्र की सहजता, संगीतात्मकता और भावात्मकता की विरासत को उसने पूरी तरह गवाँ नहीं दिया, वरन् उसे एक नए रूप में, परिष्कृत कर प्रस्तुत कर दिया। नाद, लय, छन्द के रूप में संगीतात्मकता कविता की पूरी बुनावट में बनी रही, इसीलिए वह सदैव अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रख पायी। विश्व-विख्यात कवि-कथाकार एडगर एलन पो ने कहा है, ‘‘संगीत का जब किसी प्रीतिकार कल्पना से संयोग होता है, तो वह कविता बन जाती है। संगीतरहित कल्पना, अपनी स्पष्टता अथवा निश्चितता के कारण गद्य का रूप धारण कर लेती है।’’ चूँकि मन की गहनतम भावना का संगीत से निकट का संबंध है, इसीलिए संगीत समीक्षक मीयर ने यहाँ तक कहा कि ‘‘कविता संगीत है और संगीत ध्वनिमय कविता !’’ हालाँकि यह निष्कर्ष सामान्य कविता पर भी लागू होता है, लेकिन वस्तुत: गीत ही इस कसौटी पर सर्वाधिक खरा उतरता है।
मीयर की यह धारणा भी विचारणीय है कि ‘‘कविता, आदिम मानव की सहज, अविवक्षित चिल्लाहट या पुकार मात्र थी। भय, उल्लास, आश्चर्य, अवसाद या प्रेम के अप्रत्याशित आवेश को लयबद्ध ध्वनियों या गीत-क्रमों में अभिव्यक्त किया जाने लगा और यही कविता का आदि स्वरूप था। ये ध्वनियाँ मूल रूप में शब्दार्थविहीन थीं। बाद के युग में विकसित गीतों में उनके अवशेष, उन्हीं के बीच समाविष्ट हो गये।’’
कविता में गीत को ‘आवेगमय भावनाओं का स्वत:स्फूर्त उफान’ भी कहा गया है। अंग्रेज़ी के सुप्रसिद्ध कवि पी.बी. शेली ने कहा है, ‘‘काव्य कोई तर्क-शक्ति नहीं, जो स्वेच्छापूर्वक काम में लायी जा सके। कोई कवि यह नहीं कह सकता कि मैं कविता रचूँगा, बड़ा कवि तो और भी ऐसी बात नहीं कह सकता। रचना करने वाली शक्ति तो भीतर वे वैसे ही आती है, जैसे फूल का रंग फूल के विकास के साथ-साथ ढलता और बदलता रहता है तथा हमारी चेतन शक्तियाँ, उस अदृश्य प्रभाव का न आना जानती है और न जाना।’’ और इसीलिए कवि-कर्म आसान नहीं। सर्वसुलभ भी नहीं। यह क्षमता सहज उपलब्ध नहीं होती, उसके लिए गहन-सघन, अनवरत साधना की आवश्यकता होती है। तपना पड़ता है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन में कहा भी है :
‘‘तप रे मधुर-मधुर मन
विश्व वेदना में तप प्रतिपल
जग-जीवन की ज्वाला कोमल
अपने सजल-स्वर्ण से पावन
रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम
स्थापित कर जंग में अपना मन,
ढाल रे ढल आतुर मन।’’
विश्व वेदना में तप प्रतिपल
जग-जीवन की ज्वाला कोमल
अपने सजल-स्वर्ण से पावन
रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम
स्थापित कर जंग में अपना मन,
ढाल रे ढल आतुर मन।’’
यहाँ कविता और गीत की रचना को एकरूप देखकर मैं कहना चाहूँगा कि गीत-रचना एक साधना भी है और सिद्घि भी। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य-संग्रह सांध्यगीत की भूमिका के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है; इसमें कवि को संयम की परिधि में बँधे हुए जिस भावातिरेक की आवश्यकता होती है, वह सीज प्राप्य नहीं..वास्तव में गीत के कवि को आर्तक्रंदन के पीछे छिपे हुए दु:खातिरेक को दीर्घ नि:श्वास में बँधे हुए संयम में बाँधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में सफल हो सकेगा।’’
संयम में बँधी हुई यही आत्माभिव्यक्ति या व्यक्तित्व-प्रक्षेपण समग्र कला विधाओं का अनिवार्य अंग है, लेकिन-गीत विधा में वह पराकाष्ठा पर पहुँचा होता है। गीत-रचना के दौरान बुद्धि अनुभूति उत्तेजित रहती है और अनुभूति बुद्धि से प्रोद्भासित। विचार, भाव, अनुभूति और अभिव्यक्ति की अभिन्नता एवं एकरूपता गीत विधा की विशिष्टता है और यह विशिष्टता गीतकार को अपने चतुर्दिक् के विश्व और उससे भी परे की एक स्थिति में, उस विशिष्ट रचना-काल के लिए ही क्यों न हो, ले जाती है। कवि स्टीफ़ेन स्पेंडर ने कहा है कि, ‘‘काव्य-रचना के क्षणों में मैं जिस शब्द-संगीत को साधने का उपक्रम करता हूँ, वह मुझे कभी-कभी शब्दों से परे ले जो प्राय: शब्दशून्य होती है।’’ और इस अवस्था में बार-बार पहुँचने के लिए गीतकार छटपटाता है, अन्तर्द्वन्द्वों से जूझता है, बाहरी संघर्षों का सामना करता है और इस संघर्ष को गीत में ध्वनित करता है। गीतकार रवीन्द्र भ्रमर ने झरबेर के कँटीले पेड़ पर गाने के अभ्यासी वनपाखी से तादात्मय कर रहा है :
संयम में बँधी हुई यही आत्माभिव्यक्ति या व्यक्तित्व-प्रक्षेपण समग्र कला विधाओं का अनिवार्य अंग है, लेकिन-गीत विधा में वह पराकाष्ठा पर पहुँचा होता है। गीत-रचना के दौरान बुद्धि अनुभूति उत्तेजित रहती है और अनुभूति बुद्धि से प्रोद्भासित। विचार, भाव, अनुभूति और अभिव्यक्ति की अभिन्नता एवं एकरूपता गीत विधा की विशिष्टता है और यह विशिष्टता गीतकार को अपने चतुर्दिक् के विश्व और उससे भी परे की एक स्थिति में, उस विशिष्ट रचना-काल के लिए ही क्यों न हो, ले जाती है। कवि स्टीफ़ेन स्पेंडर ने कहा है कि, ‘‘काव्य-रचना के क्षणों में मैं जिस शब्द-संगीत को साधने का उपक्रम करता हूँ, वह मुझे कभी-कभी शब्दों से परे ले जो प्राय: शब्दशून्य होती है।’’ और इस अवस्था में बार-बार पहुँचने के लिए गीतकार छटपटाता है, अन्तर्द्वन्द्वों से जूझता है, बाहरी संघर्षों का सामना करता है और इस संघर्ष को गीत में ध्वनित करता है। गीतकार रवीन्द्र भ्रमर ने झरबेर के कँटीले पेड़ पर गाने के अभ्यासी वनपाखी से तादात्मय कर रहा है :
‘‘पंछी में गाने का गुन है
दो तिनके चुन कर
वह तृप्त जहाँ होता है
गीतों की कड़ियाँ
गीतों की कड़ियाँ
बोता है !......
....कँटीली टहनी, सूखे पेड़
बियावान, सुनसान
उसे नहीं तन में
चुभी हुई है
कोई वंशी
उसके रोम-रोम में
सुरवाले मीठे सपने पलते हैं !’’
दो तिनके चुन कर
वह तृप्त जहाँ होता है
गीतों की कड़ियाँ
गीतों की कड़ियाँ
बोता है !......
....कँटीली टहनी, सूखे पेड़
बियावान, सुनसान
उसे नहीं तन में
चुभी हुई है
कोई वंशी
उसके रोम-रोम में
सुरवाले मीठे सपने पलते हैं !’’
गीत की इस यात्रा-कथा में प्रारंभ से देखें, तो उसके पाठ और उसकी रचना में लय भी लगातार जुड़ी रही और लयात्मकता उसका अनिवार्य अंग रही, जिसके साथ प्रारंभ में ध्वनि-लय का महत्त्व रहा। ध्वनि के साथ शब्द जुड़ा और शब्द की लय (रिद्म आफ़ वर्ड्स) महत्त्वपूर्ण हो उठी। नई कविता तक आते-आते उसकी लय उसके आंतरिक रचाव में पैठकर ‘अर्थ की लय’ यानी रिद्म ऑफ़ मीनिंग में परिवर्तित हो गई। अर्थ ही लय को भी समय-संदर्भों ने बदला और उसमें व्यापकता आई, जिसे गीत के नव्यतम रूप ‘नवगीत’ में रूपायित देखा जा सकता है। सुविधा के लिए हम इसे सह-संबंधों की लय (रिद्म ऑफ़ कोरिलेशन) का नाम दे सकते हैं। इन संबंधों में व्यक्ति का प्रकृति, परिस्थिति और परिवेश तीनों से संबंध है। प्रकृति या परिस्थितियों से भी संबंध है और परिवेश का व्यक्ति और प्रकृति से संबंध भी है।
इन संबंधों का एक चेहरा गीत में आज के जीवन की त्रासद स्थितियों में है, जिसे आज के नवगीतकार लोक से उठाए मुहावरे के साथ सटीक भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। उन त्रासद स्थितियों के चित्रण में भी आपको एक लय पिरोयी मिलती है, जिसे पीड़ा की लय कहा जा सकता है- रिद्म ऑफ़ टार्चर।
इसमें से कोई भी लय विखंडित होती है, तो गीत अपने विन्यास में ही उसे ध्वनित कर देता है। आज के जीवन की विडंबनाएँ, भले ही वे राजनीतिक हों, सांस्कृतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों अथवा आंतरिक मानवीय संबंधों की हों, गीत इनकी विखंडित लय को बख़ूबी वामी देता रहा है और दे रहा है। बच्चन जी ने लय की इस अनिवार्य उपस्थिति को यों व्यक्त किया है :
‘‘भाव की तीव्रता और उसकी एकता से गीत आज भी मुक्त नहीं है। इस आधार पर मुक्त छंद में लिखी बहुत-सी कविताएँ गीत की कोटि में आएँगी। यही भाव की तीव्रता और एकता उस लय को जन्म देगी, जो गीत का प्राण है और जिससे मुक्त छंद भी छुटकरा नहीं पा सकता।’’
गीत के सच्चे जानकार और हितैषी को गीत में लय टूटती नज़र आती है, तो वह समूची विधा को लेकर चिंतित होने लगता है।
इन संबंधों का एक चेहरा गीत में आज के जीवन की त्रासद स्थितियों में है, जिसे आज के नवगीतकार लोक से उठाए मुहावरे के साथ सटीक भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। उन त्रासद स्थितियों के चित्रण में भी आपको एक लय पिरोयी मिलती है, जिसे पीड़ा की लय कहा जा सकता है- रिद्म ऑफ़ टार्चर।
इसमें से कोई भी लय विखंडित होती है, तो गीत अपने विन्यास में ही उसे ध्वनित कर देता है। आज के जीवन की विडंबनाएँ, भले ही वे राजनीतिक हों, सांस्कृतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों अथवा आंतरिक मानवीय संबंधों की हों, गीत इनकी विखंडित लय को बख़ूबी वामी देता रहा है और दे रहा है। बच्चन जी ने लय की इस अनिवार्य उपस्थिति को यों व्यक्त किया है :
‘‘भाव की तीव्रता और उसकी एकता से गीत आज भी मुक्त नहीं है। इस आधार पर मुक्त छंद में लिखी बहुत-सी कविताएँ गीत की कोटि में आएँगी। यही भाव की तीव्रता और एकता उस लय को जन्म देगी, जो गीत का प्राण है और जिससे मुक्त छंद भी छुटकरा नहीं पा सकता।’’
गीत के सच्चे जानकार और हितैषी को गीत में लय टूटती नज़र आती है, तो वह समूची विधा को लेकर चिंतित होने लगता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book